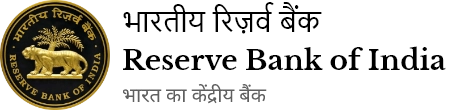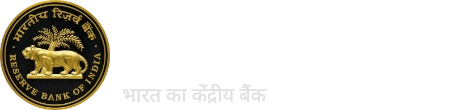IST,
IST,


रिज़र्व बैंक ने ग्रीष्मकालीन सामयिक पेपर 2011 का अंक जारी किया
7 फरवरी 2012 रिज़र्व बैंक ने ग्रीष्मकालीन सामयिक पेपर 2011 का अंक जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ग्रीष्मकालीन सामायिक पेपर 2011 अंक जारी किया। यह भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुसंधान जर्नल है। इसमें स्टाफ द्वारा लिखे गए लेख होते हैं जो लेखकों के विचार व्यक्त करते हैं। यह अंक कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में है जो नीतिगत चर्चाओं में प्रमुख स्थान बनाए हुए हैं। विदेश स्थित भारतीय बैंकों और भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की तकनीकी कुशलता की तुलना : ए स्टोकैस्टिक आउटपुट डिस्टैन्स फंक्शन दृष्टिकोण विवेक कुमार, विशाल मौर्य तथा सुजीश कुमार एस. द्वारा लिखित 'कम्पेयरिंग द टैक्निकल एफिशिएन्सी आफ़ इंडियन बैंक्स आपरेटिंग अब्रोड एण्ड फारेन बैंक्स आपरेटिंग इन इंडिया' :ए स्टोकैस्टिक आउटपुट डिस्टैन्स फंक्शन एप्रोच नामक पर्चे में विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की तकनीकी कुशलता की तुलना की गयी है और यह उनकी तकनीकी कुशलता के संबंध में देश के खुलेपन तथा स्वामित्व पैटर्न के प्रभाव की भी जांच करता है। इसके अतिरिक्त, पर्चे में इस बात पर भी चर्चा की गयी है कि क्या विकसित देशों तथा विकासशील देशों में कार्यरत बैंकों की तकनीकी कुशलता का स्तर अलग-अलग है। परिणाम से पता चलता है कि भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की तुलना में विदेश में कार्यरत भारतीय बैंक कहीं अधिक कुशल हैं और विकासशील देशों में कार्यरत बैंकों की तुलना में विकसित देशों में कार्यरत बैंक अधिक कुशल हैं। देश के खुलेपन तथा भारत से बाहर कार्यरत भारतीय बैंकों के स्वामित्व पैटर्न का उनकी तकनीकी कुशलता पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के लिए बचत, निवेश तथा आर्थिक वृद्धि के बीच संबंध – सम्बंध का क्या अभिप्राय है? रमेश जांगीली द्वारा लिखित ''कॉज़ल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग, इन्वेस्टमेंट एण्ड इकॉनॉमीक ग्रोथ फार इंडिया – वॉट डज द रिलेशन इम्प्लाय?'' पर्चे में समग्र स्तर पर तथा क्षेत्रवार स्तर पर 1950-51 से 2007-08 तक भारत के लिए बचत, निवेश तथा अर्थिक वृद्धि के बीच संबंध की जांच की गयी है। यह प्रमाणित किया जा सकता है कि भारत में इनके बीच कोई परस्पर कारण वाला संबंध नहीं है। कारण संबंधी दिशा बचत और निवेश के कारण सामूहिक रूप से तथा अलग-अलग तौर पर आर्थिक वृद्धि के बीच है और आर्थिक वृद्धि से बचत तथा (या) निवेश के बीच कोई कारणवाला संबंध नहीं है। परिणाम यह भी दिखलाते हैं कि निजी क्षेत्र की बचत तथा निवेश और आर्थिक वृद्धि के बीच परस्पर कारणवाला संबंध है। यह परस्पर कारणवाला संबंध घरेलू क्षेत्र में दिखायी दिया, जहां बचत और निवेश के कारण वृद्धि हुई और वृद्धि के कारण बचत और निवेश हुआ। पर्चे के अनुसार इस बात का प्रमाण है कि निजी कंपनी क्षेत्र की बचत के कारण आर्थिक वृद्धि नहीं होती। लेकिन इस क्षेत्र की बचत और निवेश के चलते आर्थिक वृद्धि होती है और आर्थिक वृद्धि के कारण इस क्षेत्र में बचत और निवेश होता है। पर्चे का निष्कर्ष यह है कि (i) हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश के लिए खुली है, लेकिन अभी भी वृद्धि देशी बचत के कारण होती है तथा (ii) कुछ और अधिक लाभप्रद नवोन्मेषी परियोजनाओं के लिए स्थानीय फर्में उस प्रौद्योगिकी को अपना नहीं रहीं जो विदेशी निवेश के माध्यम से आती है। क्या बचत और निवेश परस्पर जुड़े हैं? ए क्रॉस कन्ट्री विश्लेषण ''आर सेविंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कोइन्टेग्रेटेड? ए क्रॉस कन्ट्री अनालिसीस'' नामक पर्चे में संजीब बारदलई तथा जॉयस जॉन ने तीन विविध अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि यूएस, यूके तथा चीन में बचत तथा निवेश के बीच संबंध पर चर्चा की है और उसकी तुलना भारत से की है। यह देखा गया है कि सभी चारों अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि यूएस, यूके, चीन तथा भारत में बचत और निवेश परस्पर जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि निवेश पर बचत का दीर्घावधि कोइफीसिएन्ट दिखलाता है कि इन सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए (फेल्डस्टेन-होरीओका) एफएच धारणा मान्य है। विश्लेषण यह भी दिखलाता है कि अपने अधिकांश निवेश के लिए भारत स्वयं अपनी बचत पर निर्भर करता है। यूएस के लिए, हालांकि बचत और निवेश परस्पर जुड़े दिखलायी दिये, लेकिन दीर्घावधि बचत कोइफीसिएन्ट अन्य देशों की तुलना में निम्नतर पाया गया। चीन में, 2003 तक निवेश पर बचत का दीर्घावधि को एफीशिएन्ट क्रमिक रूप से बढ़ा। इसका कारण निवेश के चलते उच्च देशी बचत हो सकता है। 2004 से 2008 तक कोइफीसिएन्ट में गिरावट आयी। यह इस तथ्य के अनुरूप ही है कि इस अवधि में निवेश वृद्धि की तुलना में चीन की देशी बचत तेजी से बढ़ी। संकट से पूर्व की अवधि में यूएस तथा यूके में दीर्घावधि बचत कोइफीसिएन्ट में गिरावट दिखलाई दी, जो संकट की अवधि में बाद में बढ़ गई। विशेष नोट विशेष नोट खंड के अधीन, दीरघाऊ केशव राउत द्वारा लिखित ''स्ट्रक्चरल प्राब्लेम्स एण्ड फिसकल मॅनेजमेंट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया'' नामक पर्चे में 1960 से लेकर पिछले पांच दशकों में प्रमुख राजकोषीय वेरिएबल की दीर्घावधि की प्रवृत्ति के आधार पर राज्य सरकारों की राजकोषीय समस्याओं तथा राजकोषीय प्रबंधन का विश्लेषण किया गया है। पर्चे से पता चलता है कि संघटनात्मक समस्याएं जैसे कि वर्टिकल राजकोषीय असंतुलन, विभिन्न राज्यों में कुछ करों में विभिन्नता तथा निम्नतर गैर-कर राजस्व के कारण अभी भी मौजूद हैं और उन पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि, 1980 के दशक के उत्तरार्ध से 2003-04 तक राज्यों का राजकोषीय प्रबंधन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन 2004-05 से किये गये राजकोषीय सुधारों के कारण राज्यों को अपने वित्त का प्रबंधन करने में सहायता मिली। लेकिन, स्थूल आर्थिक मंदी और छठे वेतन आयोग के कारण वेतन संशोधन के प्रभाव के चलते, 2008-09 तथा 2009-10 में राजकोषीय सुधार में बाधा आई लेकिन 2010-11 में राज्य बजटों ने अपना राजकोषीय समेकन फिर से प्रारंभ कर दिया। पर्चे में राज्यों की राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गयी है। पुस्तक समीक्षा एन.सी.प्रधान ने इमद ए. मूसा द्वारा लिखित और पालग्रेव मॅकमिलन स्टडीज़ इन बैंकिंग एण्ड फाइनान्शिएल इंस्टिट्यूशन्स, यूके द्वारा प्रकाशित ''द मिथ ऑफ टू बीग टु फेल'' नामक पुस्तक की समीक्षा की। पुस्तक में दस अध्याय हैं और यह टू-बिग-टु-फेल धारणा तथा संबंधित मुद्दों जैसे कि लाइजेस फेयर वित्त, व्यापक अविनियमन की प्रवृत्ति,तथा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र की स्थिति के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखती है। यह न केवल प्रथा की आलोचना करती है बल्कि उन विचारों की भी आलोचना करती है जो प्रथा को जन्म देते हैं – जिनमें से कुछ शैक्षणिक कार्य के कारण होते हैं। पुस्तक में अधिकांश चर्चा यूनाइटेड स्टेट्स की गतिविधियों के बारे में है, जहां जमाराशि बीमा ने जन्म लिया और टीबीटीएफ शब्द को इजाद किया गया। टीबीटीएफ को हतोत्साहित करने के लिए, पुस्तक का यह मानना है कि प्रतिबंधों तथा प्रोत्साहनों के माध्यम से विशालता तथा जटिलता से जुड़े बाह्य तथ्यों को आत्मसात करने का विकल्प उपलब्ध है, दूसरा विकल्प है संस्थाओं के आकार को नहीं बल्कि उनके विफल हो जाने की संभावना को ध्यान में रखना। पुस्तक इस बात पर बल देती है कि सरकार द्वारा जीवनदान के बिना तथा करदाता के पैसे से वित्तपोषित विफल होती हुई फर्म को जीवित रखना वांछनीय नहीं है। अरविंद के. झा ने कार्ल पी.सौवंत, जया प्रकाश प्रधान, आएशा चटर्जी तथा ब्राएन हार्ले द्वारा संपादित तथा पालग्रेव मैकमिलन, न्यू यार्क द्वारा प्रकाशित ''द राइज़ ऑफ इंडियन मल्टीनैशनल्स : परस्पेक्टिव ऑफ़ इंडियन आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट'' नामक पुस्तक की समीक्षा की है। पुस्तक में नौ अध्याय हैं जिनमें प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगमों की उन्नति के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण दिये गये हैं। पुस्तक में भारतीय बहुराष्ट्रीय निगमों के संबंध में प्रवृत्ति और मुद्दों का प्रखर विश्लेषण किया गया है। भारतीय बहुराष्ट्रीय निगमों की त्वरित वृद्धि पर चर्चा करते हुए, पुस्तक पैटर्न तथा कारकों के आधार पर उन विभिन्न दृष्टिकोणों का उल्लेख करती है जिनके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी उपस्थिति बढ़ी। एक अध्याय में, ओएफडीआई में उल्लेखनीय वृद्धि का विश्लेषण तीन बातों के आधार पर किया गया है अर्थात्, ओएफडीआई की गति और दिशा, ओएफडीआई के पीछे स्वामित्व लाभ तथा उद्देश्य में मूल देश की भूमिका। ये तीनों स्पष्टीकरण हाल ही में ओएफडीआई के डायनॉमिक्स के बारे में अंशत: स्पष्टीकरण देते हैं। एक और अध्याय ओएफडीआई के लिए सरकारी नीतियों की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भूमिका के बारे में चर्चा करता है। एक अध्याय में यह बताया गया है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय निगमों की सफलता उनके कांग्लोमैरेट संघटन के कारण है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए कुछ स्पष्ट संदेश भी दिये गये हैं। समीक्षा में पुस्तक में कुछ अनुपलब्ध सूत्रों पर भी बल दिया गया है। जे. डी. देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1265 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: