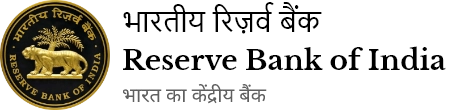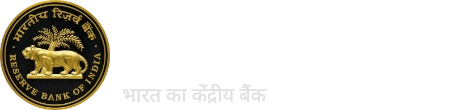IST,
IST,


भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश पर चर्चा पेपर पर अभिमतों का सारांश जारी किया
|
23 दिसंबर 2010 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश पर चर्चा पेपर पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर "निजी क्षेत्र में नए बैंकों का प्रवेश" पर चर्चा पेपर पर अभिमतों का सारांश जारी किया। प्राप्त अभिमतों में काफी विभिन्नताएं है और किसी भी विषय पर एक स्पष्ट राय प्राप्त नहीं हुई। प्राप्त अभिमत क्षेत्रीय स्थिति अर्थात् बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और औद्योगिक गृहों के विचारों को दर्शाते हैं। अन्य अभिमतों में भी काफी विभिन्नताएं थीं। आपको यह याद होगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11 के लिए अपने बज़ट भाषण में यह घोषणा की थी कि रिज़र्व बैंक निजी क्षेत्र के सहभागियों को कुछ अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार कर रहा है। इसके अनुसरण में वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने यह दर्शाया था कि रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रणालियों, भारतीय अनुभव और मौजूदा स्वामित्व तथा विनियामक दिशानिर्देशों को शामिल कर एक चर्चा पेपर तैयार करेगी तथा चर्चा पेपर को जुलाई 2010 तक व्यापक अभिमत और प्रतिसूचना के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी करेगी। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 अगस्त 2010 को पेपर बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक गृहों, अन्य संस्थाओं तथा खासकर जनता से सुझाव/अभिमत प्राप्त करने अपनी वेबसाइट पर 'निजी क्षेत्र में नए बैंकों का प्रवेश' पर चर्चा पेपर जारी किया था। चर्चा पेपर में निम्नलिखित विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय अनुभव तथा प्रत्येक दृष्टिकोण के मतों-अभिमतों सहित संभाव्य दृष्टिकोण की समीक्षा की गई।
उपर्युक्त विषयों पर उद्योग, बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्त संस्थानों के शेयरधारकों के संगठनों तथा भारतीय उद्योग परिसंघ, एएसएसओसीएचएएम, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ, भारतीय बैंक संघ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों का संगठन, एफआइडीसी, एमएफआइएन, अर्नस्ट एण्ड यंग और प्राइस वॉटर हाऊस कूपर्स जैसे कुछ सलाहकारों के साथ 7 और 8 अक्टूबर 2010 को विस्तृत चर्चा की गई थी। साथ ही, चर्चा पेपर पर व्यापक संख्या में अभिमत प्राप्त हुए जिनमें वे सहभागी जो नए बैंक स्थापित करना चाहते है, उद्योग संगठनों, बैंकों, शिक्षाविदों, बैंकिंग और वित्त से जुड़े प्रख्यात व्यक्तियों तथा आम जनता शामिल थे। अभिमतों का सारांश मेल तथा चर्चा के माध्यम से महत्वपूर्ण शेयरधारकों तथा प्रख्यात व्यक्तियों से विभिन्न विषयों पर प्राप्त अभिमतों का सारांश निम्नानुसार है : (क) नए बैंकों के लिए न्यूनतम पूँजी आवश्यकता निजी क्षेत्र में स्थापित की जानेवाली नई बैंकों की प्रारंभिक न्यूनतम पूँजी आवश्यकता पर विभिन्न मत रखे गए। सामान्यत: उद्योग/बैंकों के संगठन/संघ ₹1000 करोड़ की उच्च शुरूआती पूँजी के पक्ष में थे जिसे समयावधि के दौरान ₹1500 करोड़ से ₹2000 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। उनका मानना था कि नई बैंकों को वित्तीय समावेशन और कार्यशील रहने के लिए परिचालनों को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी में उच्चतर निवेशों की आवश्यकता होगी। साथ ही, न्यूनतम पूँजी का उच्च स्तर से यह सुनिश्चित होगा कि केवल गंभीर सहयोगी ही जिनका दीर्घावधि विज़न होगा बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी/लघु वित्त संस्थान क्षेत्र ₹300 करोड़ से ₹500 करोड़ तक की न्यूनतम शुरूआती पूँजी चाहते थे। उनका यह मत था कि इस पूँजी आवश्यकता से वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रीत करते हुए अगले 5 से 10 वर्ष की अवधि में लगभग 30 से 40 बैंकों को लाइसेंसिकृत किया जा सकता है। एक मत यह भी था कि ₹1000 करोड़ की पूँजी वाला बड़ा बैंक स्थानीय उधार अथवा वित्तीय समावेशन में इतना प्रभावी नहीं हो सकता है और इसीलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ₹50 करोड़ की न्यूनतम पूँजी और 15 प्रतिशत से अधिक पूँजी का आस्ति अनुपात वाली लगभग 20 नई बैंकों को प्रतिबंधित (पारंपारिक) बैंकिंग लाइसेंस जारी करने पर विचार कर सकती है। (ख) नए बैंकों में प्रवर्तक की शेयरधारिता प्रारंभिक प्रवर्तक (प्रमोटर्स) का अंशदान 30 से 100 प्रतिशत तक रखे जाने का सुझाव था। उद्योग के संगठनों/संघों का सुझाव 40 से 51 प्रतिशत तक रखने का सुझाव था जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/लघु वित्त संस्थानों का 30 से 40 प्रतिशत का निम्नतर रखे जाने का सुझाव था। प्रमोटर्स का न्यूनतम अंशदान स्टेक को कम करने के बाद उसे 5 से 26 प्रतिशत तक 5 से 10 वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। औद्योगिक प्रतिनिधियों का यह मानना था कि मज़बूत कंपनियॉं प्रमोटर चालित होती है और इसीलिए अंतिम स्टेक धारिता 20 से 26 प्रतिशत की होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रमोटरों की रूचि और प्रतिबद्धता लंबे समय तक बनी रहे। यह सुझाव था कि कैनेडियन नमूने की तरह बैंक के विस्तार के अनुसार प्रमोटर को ₹1000 करोड़ की प्रारंभिक पूँजी वाले बैंकों के मामले में 40 प्रतिशत, ₹1000 से ₹2000 करोड़ की पूँजी वाले बैंकों के मामले में 30 प्रतिशत तक और ₹2000 करोड़ से अधिक की पूँजी वाले बैंकों के मामले में 10 से 20 प्रतिशत तक अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरा सुझाव था कि प्रमोटर का अंशदान मताधिकार के प्रतिबंध के साथ 40 से 50 प्रतिशत तक जारी रखा जाए ताकि नियंत्रण से संबंधित मामलों को संबोधित करते हुए प्रमोटर की आर्थिक रूचि सुनिश्चित की जाए। लघु वित्त क्षेत्र से यह सुझाव था कि दीर्घावधि में प्रमोटर की धारिता पर 10 प्रतिशत की निम्न सीमा हो ताकि यह सुनिश्चित किया जाए की बैंक व्यक्तिगत रूप से चालित होने के बजाए अनुसूची चालित हो। (ग) नई बैंकों में विदेशी शेयर धारिता विदेशी शेयर धारिता के संबंध में शेयर धारिता को 50 प्रतिशत तक रखने से लेकर बिलकुल कोई प्रतिबंध ही नहीं जैसे कई सुझाव आए थे। उद्योग/संगठनों/बैंकों में भी जबकि कुछ ने 50 प्रतिशत की सीमा रखने की हिदायत दी, दूसरों ने यह सुझाव दिया कि 74 प्रतिशत का वर्तमान मानदण्ड जारी रखा जाए अथवा 10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए कोई प्रतिबंध न हो। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/लघु वित्त संस्था क्षेत्र का यह मानना था कि बैंकिंग उद्योग के लिए 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करना विरोधात्मक होगा क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में विदेशी निवेशों के लिए 100 प्रतिशत की अनुमति है। वे 74 प्रतिशत के वर्तमान मानदण्ड को बनाए रखने अथवा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाने के पक्ष में थे। जनता से प्राप्त और एक सुझाव यह था, मताधिकार पर प्रतिबंध लगाना जो एकल रूप में 5 प्रतिशत और समग्र रूप में 26 प्रतिशत अथवा निर्धारित की गई अन्य कोई सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। (घ) नई बैंकों को प्रमोट करने वाले औद्योगिक/व्यवसाय गृह क्या औद्योगिक/व्यवसाय गृहों को नई बैंकों को प्रमोट करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं पर विभिन्न अभिमत प्राप्त हुए। इनमें उनको अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए और यदि हॉं तो किसे अनुमति दी जानी चाहिए और किन शर्तों पर इत्यादि शामिल था। उद्योग के संगठन/संघ तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियॉं/लघु वित्त संस्थाएं सामान्य रूप से नई बैंकों को प्रमोट करने के लिए औद्योगिक/व्यवसायी गृहों को अनुमति देने के पक्ष में थी। दूसरी ओर अन्य ने भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया है कि औद्योगिक गृहों को बैंकिंग में प्रवेश देने के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए तथा औद्योगिक गृहों को बिना किसी प्रतिबंध के बैंकिंग लाइसेंस नहीं देना चाहिए। भारत और विदेश में पूर्व अनुभवों को देखते हुए मौजूदा बैंक भी इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थीं। उनका यह मानना था कि औद्योगिक/व्यवसायी गृहों द्वारा प्रायोजित बैंकों को उपलब्ध होनेवाली अत्यधिक पूँजी के कारण मौजूदा बैंकों के साथ असंतुलित सहभागिता होने की संभावना होगी। तर्कवितर्क के प्रमुख मुद्दे निम्नानुसार है: (i) औद्योगिक/व्यवसायी गृहों को लाइसेंस न देने संबंधी तर्कवितर्क
(ii) औद्योगिक/व्यवसायी गृहों को लाइसेंस प्रदान करने के पक्ष में तर्कवितर्क
(iv) औद्योगिक/व्यवसायी गृहों को नई बैंकों को प्रायोजित करने की अनुमति के लिए सुरक्षा जॉंच
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों में परिवर्तन अथवा नए बैंकों के प्रवर्तन की अनुमति के मामले पर अलग-अलग विचार थे। एक अग्रणी उद्योग संघ की राय थी कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग के प्रति इसकी कारोबारी प्रतिदर्श को समरूप बनाने में कठिनाई के कारण प्रवर्तन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तथापि, यदि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नए बैंक प्रवर्तित करने की अनुमति दी जाती है तो उनसे यह कहा जाए कि वे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में हल्के विनियमनों के कारण अधिनिर्णय अवसरों को समाप्त करने के लिए चरणबद्ध् तरीके से उन गतिविधियों को बंद करें जिसे बैंक कर सकते हैं। अन्य उद्योग संघ सामान्यत: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के परिवर्तन अथवा उनके द्वारा नए बैंकों के प्रवर्तन के पक्ष में थे। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी/माइक्रो वित्त संस्था क्षेत्र दोनों विकल्पों के पक्ष में थे। बैंक केवल अकेले कारोबार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा नए बैंकों के प्रवर्तन की अनुमति देने के पक्ष में थी और उसी समय औद्योगिक/घरानों द्वारा प्रायोजित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर रोक लगाना चाहते थे। (च) कारोबारी प्रतिदर्श उद्योग संघों और बैंकों की प्रभावी राय यह थी कि सामान्य बैंकिंग लाइसेंस नए खिलाडि़यों को समान कारोबारी क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए दिए जाएं। किसी भौगोलिक क्षेत्र अथवा वित्तीय समावेशन जैसे कारोबारी स्वरूप में संक्रेंदण एक अव्यवहारर्य प्रस्ताव होगा। वित्तीय समावेशन बाज़ार संचालित होना चाहिए लेकिन उसका निर्धारण नहीं होना चाहिए। चूँकि बैंकों को वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के साथ चलने तथा सीआरआर, एसएलआर, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम निर्धारण आदि का अनुपालन करने की भी ज़रूरत होती है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नए बैंकों को निश्चित समयावधि दिए जाने की ज़रुरत है। चूँकि नए बैंकों को लाइसेंस स्वीकृत करने का उद्देश्य वित्तीय समावेशन है, नए बैंकों को एक अलग प्रकार का लाइसेंस दिया जा सकता है। एक विख्यात अर्थशास्त्री ने सुझाव दिया है कि प्रारंभिक अवधि में उनकी गतिविधियॉं अधिक पारंपरिक बैंकिंग तक सीमित रखी जा सकती है जिसमें पर्यवेक्षकों को बैंकों में विश्वास प्राप्त करते ही रियायत दी जा सकती है। संपूर्ण रूप से बैंकिंग लाइसेंस कतिपय मानदण्डों के अनुपालन अधीन तीन वर्षों के परिचालन के बाद दिए जा सकते हैं। यह सुझाव भी थे कि नए बैंक छोटे ऋणवाले वित्तीय उत्पादों के लिए ऋण के आकार से संबंधित स्पष्ट परिभाषा के साथ काम करें। तथापि, उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने की ज़रूरत नहीं है जिनमें नए बैंक काम करेंगे क्योंकि महानगरों और बड़े नगरों में भी वित्तीय रूप से वंचित लोग हैं। आर. आर. सिन्हा प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/883 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: