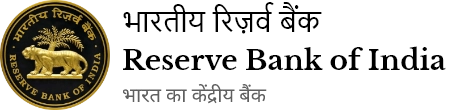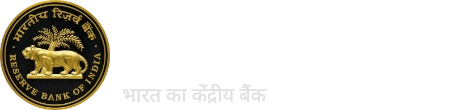|
27 अक्टूबर 2009
मौद्रिक नीति 2009-10 की दूसरी तिमाही समीक्षा पर
गवर्नर, डॉ. डी.सुब्बाराव का प्रेस वक्तव्य
"आज सुबह प्रमुख बैंकों के प्रधानों के साथ मेरी एक बैठक हुई जहाँ हाल की आर्थिक गतिविधियों पर हमने चर्चा की और जहाँ मैंने वर्ष 2009-10 के लिए रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा की घोषणा की। इस नीति समीक्षा के दौर में हमने स्टेकधारकों की व्यापक श्रेणियों से परामर्श किया और उनके विचारों को सुना।
बैंक सामान्यत: रिज़र्व बैंक के नीति रुझान का स्वागत करते हैं। वे ऋण प्रवाहों विशेषकर कृषि और व्यष्टि, लघु और मध्यम उद्यमों पर वृद्धि को पुनर्ज्जीवित करने की सहायता के लिए रिज़र्व बैंक के दबावों पर सहमत हुए। उन्होंने उल्लेख किया कि जबकि आर्थिक गतिविधि को रेखांकित करने में तेज़ी आ गई है ऋण माँग में चुप्पी बनी हुई है क्योंकि बाह्य और घरेलू गैर-बैंक स्रोतों से वित्तीय सहायता तक पहुँच उल्लेखनीय रूप से आसान हो गई है। बैंकों ने महसूस किया कि आगे चलकर ऋण वृद्धि संभावनाएँ अनुकूल बनी रहेंगी। ऋण शुरुआत के अलावा यह चर्चा विशेष मुद्दों, जैसे कि शाखा प्राधिकरण पर नई उदारीकृत नीति, प्रावधानीकरण मानदण्डों में परिवर्तन, मूलभूत सुविधा को वित्तीय सहायता, मुद्रा प्रबंध, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) और बेंचमार्क मूल उधार दर पर कार्यदल की अनुशंसाओं पर केंद्रित रही। बैंकों ने शाखा प्राधिकरण पर उदारीकृत नीति का स्वागत किया जो उनके अनुसार उदारीकृत कारोबारी प्रतिनिधि प्रतिदर्श के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन और ऋण प्रवाह में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। जहाँ तक बैंकों द्वारा मूलभूत सुविधा वित्तीय सहायता का संबंध है, यह विचार था कि जबकि बैंकों की मूलभूत सुविधा वित्तीय सहायता में एक भूमिका है अंतत: इसे दीर्घावधि संस्थागत निवेशकों की सहभागिता के साथ कंपनी बॉण्ड बाज़ार के माध्यम से किया जाना चाहिए। बैंकों ने अंतरण वित्त पोषण की भूमिका की पहचान की और उल्लेख किया कि वे इस मामले पर भारतीय मूलभूत सुविधा वित्त कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) के साथ कार्य कर रहे हैं। जबकि बैंकों ने वाणिज्यिक भू-संपदा निवेशों पर प्रावधानीकरण अपेक्षा में वृद्धि के प्रस्ताव का स्वागत किया, उन्होंने प्रावधानीकरण सुरक्षा की गणना में कतिपय संशोधन सुझाए तथा कुछ और समय की माँग की। रिज़र्व बैंक ने नोट छँटाई मशीनों सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्त्व पर बल दिया। एक सामान्य भावना थी कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों (पीएसएलएस) के गुण और दोषों की सावधानी से जाँच की जाए जैसा कि रिज़र्व बैंक ने प्रस्तावित किया है। बैंकों से आग्रह किया गया कि वे सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) पर कार्यदल की अनुशंसाओं पर चर्चा शुरू कराएं।
वैश्विक अर्थव्यवस्था
जुलाई 2009 में हुई पिछली समीक्षा के समय से वैश्विक अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर सुधार हो रहा है। यह सुधार उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर एशिया में उत्पादन विस्तार से ध समर्थित है। दूसरी तिमाही में विश्व उत्पादन में सुधार आया है, विनिर्माण गतिविधि ने ज़ोर पकड़ा है, व्यापार की स्थिति अच्छी रही है, वित्तीय बाज़ार स्थितियाँ सुधर रही हैं और जोखिम लेने की भूख वापस लौट रही है। शेयर बाज़ारों में तेज़ी से अच्छी स्थिति आने के कारण बैंकों को अपने तुलनपत्र की स्थिति सुधारने के लिए पूँजी जुटाना आसान हो गया है। तथापि, चिंताएं फिर भी हैं कि यह सुधार बड़ा कमज़ोर है। हालांकि उत्पादन फिर से ज़ोर पकड़ रहा है और बेरोज़गारी 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की संभावना है। खराब तुलनपत्रों, अधिक क्षमता और वित्तीय बाधाओं के चलते निवेश की स्थिति भी कमज़ोर बने रहने की आशा है। बैंकों का लुढ़कना जारी है। विश्व व्यापार एक वर्ष पहले के अपने स्तर से अभी भी नीचे बना हुआ है। कुल मिलाकर जहाँ वैश्विक आर्थिक संभावनाएं सुधरी हैं वहीं आर्थिक स्थिति सुधरने की गति और वहनीयता के बारे में अनिश्चितताएं कायम हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था
भारत में भी अर्थव्यवस्था के ‘पलायन वेग’ तक पहुँचने और पुन: वृद्धि की पटरी पर वापस लौटने के निश्चित संकेत दिखाई देने लगे हैं। यह सब निर्यातों के कम होने और 1972 के बाद के सबसे भयंकर सूखे की स्थिति के बावजूद है। हाल ही के महीनों में औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार आया है। देशी और विदेशी वित्तीय स्थितियों में पलटाव का रुख है। पूँजी प्रवाहों में फिर से जान आ गई है। प्राथमिक पूँजी बाज़ार की गतिविधि ने ज़ोर पकड़ लिया है और बैंक से इतर घरेलू स्रोतों से निधीयन आसान हुआ है। चलनिधि स्थितियाँ सुगम बनी रही हैं और ब्याज दरें मुद्रा एवं क्रेडिट बाज़ारों में नरम पड़ी हैं।
कुछ चिंताएं अभी भी कायम हैं। मुद्रास्फीति बढ़ने के स्पष्ट संकेत हैं और ये अधिकांशत: आपूर्ति की ओर से विशेष रूप से खाद्यान्न मूल्यों से उत्पन्न हो रहे हैं। निजी उपभोग माँग ने अभी भी ज़ोर नहीं पकड़ा है। कृषि उत्पादन में गिरावट की संभावना है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि प्रवृत्ति से नीचे बनी हुई है। बैंक क्रेडिट में वृद्धि सतत मंद है।
सरकारी उधार
बिना किसी समस्या के भारी सरकार बाज़ार उधार कार्यक्रम का प्रबंधन रिज़र्व बैंक के लिए एक प्रमुख चुनौती रही है। निभावपरक मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुरूप रिज़र्व बैंक ने इस उधार कार्यक्रम को प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए खुला बाज़ार परिचालनों (ओएमओ) और बाज़ार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) को खोलकर अपनी देशी आस्तियाँ बढ़ाईं। 2009-10 में अब तक केंद्र सरकार ने अपना निवल बाज़ार उधार कार्यक्रम 80 प्रतिशत (3,19,911 करोड़ रुपए) पूरा कर लिया है और राज्य सरकारों ने बाज़ार उधार कार्यक्रम के माध्यम से 58,683 करोड़ रुपए (निवल) जुटाए हैं। बाज़ार उधार कार्यक्रम के प्रारंभ में ही पूरा हो जाने (फ्रंट लोडिंग) के कारण 2009-10 की शेष अवधि में केंद्र सरकार के बाज़ार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत निवल अग्रिम लगभग 62,500 करोड़ रुपए ही होंगे। इस निर्गम के गुण-दोषों पर विचार करने के आधार पर बैंकों के लिए परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) निवेश सीमा बढ़ाने के विषय पर चर्चा के संदर्भ में रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि एचटीएम अनुपात बढ़ाना ठीक नहीं है।
चलनिधि की स्थिति और ब्याज दरें
चलनिधि की स्थिति नवंबर 2008 के मध्य से संतोषजनक रही जो चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), रिज़र्व बैंक के माध्यम के अन्तर्गत दैनिक आधार पर 1,20,000 करोड़ रु. के लगभग बड़ी मात्रा में खपत से स्पष्ट है। अधिकांश वाणिज्य बैंकों द्वारा अपनी जमाराशि की दरें कम करने से निधि की लागत कम हो गयी है जिससे बैंक अपनी उधार दरें कम कर पाए हैं।
वृद्धि परिदृश्य
चालू मूल्यांकन में 2009-10 के सकल देशी उत्पाद के लिए वृद्धि प्राक्कलन ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति के साथ 6.0 प्रतिशत रहा जो जुलाई समीक्षा में अपरिवर्तित रहा। इससे कृषि उत्पादन में कुछ कमी की संभावना है क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून इस वर्ष, 1972 से अबतक सबसे कमजोर रही है जिससे कृषि फसलों की आय और एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है लेकिन औाद्योगिक उत्पादन में अधिक तेजे से सुधार हुआ है।
मुद्रास्फाति परिदृश्य
थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फाति तथा विनिमय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फाति उपायों के बीच व्यापक अंतर के मद्देनजर हाल ही में मुद्रास्फाति मूल्यांकन उत्तरोत्तर जटिल हो गया है। यह स्थिति देश के कई भागों में कम वर्षा और सूखे की स्थिति से और खराब हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दो अंकों में है लेकिन थोक मूल्य सूचकांक कम रहा है।
पण्य मूल्यों में वैश्विक प्रवृत्ति और देशी मांग-आपूर्ति शेष को ध्यान में लेते हुए मार्च 2010 के अंत में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फाति का मूल अनुमान ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति के साथ 6.5 प्रतिशत पर रखा गया है। यह जुलाई 2009 की समीक्षा में अनुमानित 5.0 प्रतिशत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फाति से अधिक है। इसका कारण है ऊर्ध्वमुखी जोखिम का होना।
मुद्रा आपूर्ति
वर्ष 2009-10 की शेष अवधि में सरकार की और वाणिज्य क्षेत्र की उधार आवश्यकता को ध्यान में लेते हुए जुलाई 2009 की समीक्षा में मुद्रा आपूर्ति में निर्धारित 18 प्रतिशत की वृद्धि का सांकेतिक अनुमान संशोधित करते हुए 17 प्रतिशत रखा गया है। इसके अनुरूप अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशियों में 18 प्रतिशत तक वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। समायोजित खाद्येतर ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्ड/डिबेंचर/शेयरों और निजी कार्पोरेट क्षेत्र तथा वाणिज्यिक पत्र में निवेश सहित, में वृद्धि भी पहले निर्धारित 20 प्रतिशत से कम करते हुए 18 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। बैंकों से फरि से आग्रह किया गया है कि वे ऋण विस्तार करने के अपने प्रयास बढाएं जो वृद्धि के पुनरुज्जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।
सुधार का प्रबंध : कुछ मुद्दे
विश्वभर में और साथ ही भारत में ध्यान संकट के प्रबंध पर टिका हुआ है। निम्नलिखित कारणों से भारत के लिए नीतिगत दुविधाएं कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा साथ ही अन्य उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं से अलग हैं :
- इनमें से बहुत से देशों को मुद्रास्फीति का तत्काल जोखिम नहीं है जबकि भारत मुद्रास्फीति के सुधार के लिए सक्रिय रूप से सामना कर रहा है।
- भारत के सामने घरेलू उपभोग तथा निवेश माँग संभालने की चुनौती रही है जोकि हमारी वृद्धि के पारंपरिक, प्रमुख ड्राइवर है। यद्यपि, घरेलू वस्तुएं, भारत की फर्म और वित्तीय संस्थाएं अग्रिम अर्थव्यवस्था वाले देशों के विकृत तुलन पत्र की तरह प्रबल उद्योग नहीं कर पा रही है।
- भारत में अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से अग्रिम अर्थव्यवस्था वाले देशों, जहाँ माँग आधारित रहती है, के विपरीत नियंत्रित रूप में रही है। आपूर्ति बाध्यता जो कि कमज़ोर माँग के चलते संकट के समय नियंत्रित रूप में रही है वह अब पुन: उभरेगी और वास्तव में बाध्यकारी हो जाएगी।
- भारत बड़े पैमाने पर दो घाटे वाली उभरती अर्थव्यवस्था यथा राजकोषीय और चालू खाता घाटे वाली अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक रहा है।
निर्गमन नीति
पूरे विश्व में विस्तृत मौद्रिक स्वरूप से बाहर निकलने के समय और तरतीब पर सक्रिय रूप से वादविवाद होता रहा है। हमारे नीतिगत ढाँचे में ‘निर्गमन’ केंद्रीय मुद्दा भी रहा है। रिज़र्व बैंक के लिए चुनौती इस बात की रही है कि मूल्य स्थिरता से समझौता किए बगैर वसूली प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। वृद्धिकारक विलंब से निकलना चाहते हैं जबकि मुद्रास्फीति त्वरित निर्गम चाहती है। समय-पूर्व निर्गमन कमज़ोर वृद्धि को गड़बड़ा सकता है जबकि विलंबित निर्गमन मुद्रास्फीति संभावनाओं की संभाव्यता को बढ़ा सकता है। इसकी बज़ह से लेनदेन प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा।
मौद्रिक समृद्धि के पक्ष और विरोध के तर्क पर हमने अध्ययन किया। ये तर्क नीति समीक्षा दस्तावेज़ के लिए गए हैं। इस समय पर उचित निर्णय यह होगा कि ‘निर्गमन’ के क्रम को यथोचित रूप से इस तरह से अपनाया जाए ताकि वसूली प्रक्रिया में बर्गर कोई रुकावट लाए मुद्रास्फीति अपेक्षाएं जहाँ हैं वहीं बनी रहें।
मौद्रिक नीति रुझान
उक्त समग्र मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2009-10 के अवशेष अवधि के लिए मौद्रिक रुझान निम्नानुसार रहेगा:
- मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर सतर्क निगाह रखें तथा नीति समायोजन द्वारा प्रभावी ढँग से तत्परता पूर्वक मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए तैयार रहें।
- चलनिधि स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखना और उसका सक्रिय प्रबंधन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादक क्षेत्रों की ऋण माँग पर्याप्त रूप से पूरी करने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता भी बनाई रखी जाती है।
- मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ मौद्रिक और ब्याज दर बनाए रखना जो वृद्धि प्रक्रिया को समर्थित करे।
आगामी पथ
रिज़र्व बैंक समग्र रूप से मूल्य स्थिति पर निगरानी रखना जारी रखेगा और सामने आनेवाले समष्टि आर्थक स्थितियों द्वारा अपेक्षित शीघ्र और प्रभावी रूप से उपाय करेगा।
मौद्रिक नीति के उपाय
फिलहाल, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि नीतिगत रिपो दर को 4.75 प्रतिशत पर रिवर्स रिपो दर को 3.25 प्रतिशत पर तथा बैंकों के सीआरआर को उनकी निवल माँग और समय देयता के 5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।
‘निगर्मन’ के प्रथम चरण में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :
- सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को पहले माँग और समय देयता के 25 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत किया गया था, अब इसे पुन: 25 प्रतिशत किया जाता है।
- निर्यात ऋण पुन: वित्तपोषण सुविधा की सीमा को पात्र शेष निर्यात ऋण के 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था, अब इसे पुन: संकट-पूर्व के 15 प्रतिशत के स्तर पर लाया गया है।
- (i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु विशेष पुन: वित्त पोषण सुविधा; तथा (ii) अनूसूचित वाणिज्य बैंकों डम्यूचुअल फण्डों (एमएफ) को निधियाँ प्रदान करने के लिए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा आवास वित्तीय कंपनियों (एचएफसी) को दी जाने वाली दो अपारंपरिक वित्तपोषण सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाता है।
भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ किए जाने वाले संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) वाले देनदेनों से उत्पन्न होनेवाली अनुसूचित बैंकों की देयताएं अब नकदी आरक्षित अनुपात बनाए रखने के अधीन होंगी।
विकासात्मक विनियामक मुद्दे
अब मैं विकासात्मक तथा विनियामक मुद्दों पर आता हूँ। अन्य अधिकांश देशों के मुकाबले भारत इस संकट से कम प्रभावित हुआ है पर फिर भी भारत को इस संकट से कुछ सीख मिली है जिनमें शामिल हैं : (i) प्रणालीगत तथा संस्थागत स्तर पर विनियमन को और सुदृढ़ करना; (ii) अपने पर्यवेक्षण को और अधिक प्रभावी तथा मूल्य-संवर्धित बनाना; और (iii) जोखिम प्रबंधन में अपने कौशल को सुधारना। इसके अलावा, हमारे लिए आवश्यक है कि वित्तीय समावेशन की चुनौतियों का सक्रिय रूप से सामना किया जाए। हमने जो कुछ कार्रवाइयाँ की हैं मैं उनका उल्लेख करना चाहूँगा।
वित्तीय स्थिरता
- दिसंबर 2009 तक भारत की पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करना।
ब्याज दरें
- बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली पर गठित कार्य समूह की सिफारिशों पर फीडबैक मिलने के उपरांत विचार करना।
वित्तीय बाज़ार उत्पाद
- समुचित सुरक्षा मानकों के अधीन निवासी सत्ताओं हेतु कारपोरेट बाण्ड के लिए साधारण ओवर-दि-काउँटर (ओटीसी) एकल नामवाले क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) शुरू करने का प्रस्ताव। बाज़ार सहभागियों के साथ विचार-विमर्श करने के उपरांत परिचालन संबंधी ढाँचे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- प्रतिष्ठित शेयर बाज़ारों को वर्तमान रूपया-अमरीकी डॉलर सौदों के अतिरिक्त रुपया-यूरो, रुपया-पाउँड स्टर्लिंग, रुपया-जापानी येन के करेंसी जोड़ों में करेंसी भावी सौदों के प्रस्ताव की अनुमति दी।
विनियामक उपाय
- ‘मानक आस्तियों’ के रूप में वर्गीकृत वाणिज्य संपदा क्षेत्र को अग्रिमों के लिए आवश्यक प्रावधानीकरण को 0.4 प्रतिशत से 1.0 प्रतिशत बढ़ा दिया गया।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के घरेलू गैर-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए वर्तमान शाखा प्राधिकरण नीति को उदार बनाया गया।
- बैंकों को चरणबद्ध रूप से अंतरण वित्त पोषण निवेशों के लिए पूँजी बढ़ाने की अनुमति दी गई।
- बैंकों को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) तथा अस्थिर प्रावधानों के लिए विशिष्ट प्रावधानों वाली अपनी प्रावधानीकरण सुगमता को बढ़ाने के लिए सूचित किया गया ताकि अस्थिर प्रावधानों सहित उनका कुल प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात सितंबर 2010 तक 70 प्रतिशत हो जाए।
- सुदृढ़ क्षतिपूर्ति नीतियों के संबंध में निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को दिशा-निर्देया जारी करना।
- मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अपनी कुल आस्तियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत धारिता वाली संस्थाओं को ‘मूलभूत सुविधा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी’ के रूप में परिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की एक श्रेणी शुरू करना।
- मूलभूत सुविधा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों के निवेशों की जोखिम भारिता को बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (इसीएआइ) द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को दी गयी ऋण रेटिंग से जोड़ना।
वित्तीय समावेशन
- बैंकों को (i) कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) के रूप में अतिरिक्त संस्थाओं की नियुक्ति तथा (ii) बीसी के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहकों से यथोचित सेवा प्रभार पारदर्शी रूप से वसूल करने की अनुमति देना।
- मार्च 2011 तक 2,000 से अधिक जनसंख्यावाले प्रत्येक गांव में बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अग्रणी बैंकों को मार्च 2010 तक रूपरेखा तैयार करने के लिए कदम उठाने के संबंध में सूचित करना।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) शुरू करने में निहित मुद्दों की जांच के लिए कार्यकारी दल का गठन करना।
मुद्रा प्रबंधन
- बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में नोट सार्टिंग मशीन रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार चरणबद्ध रूप से स्थापित करने के लिए अनिवार्य करना।"
जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/632 |
 IST,
IST,