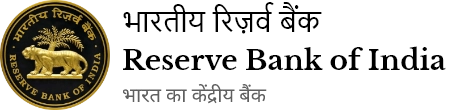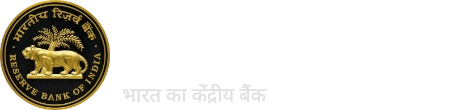IST,
IST,
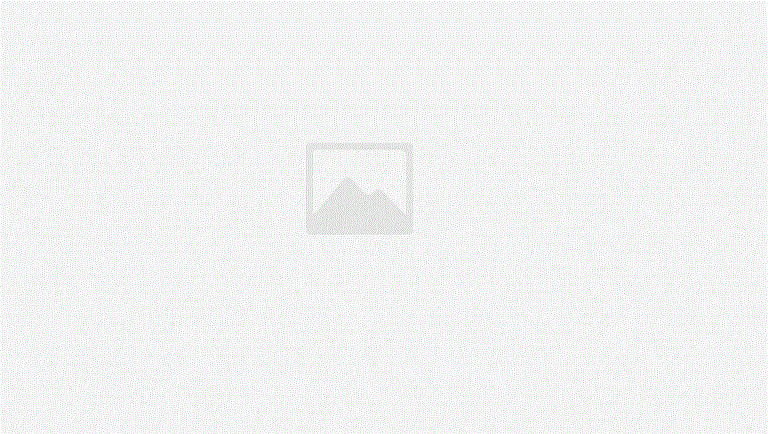
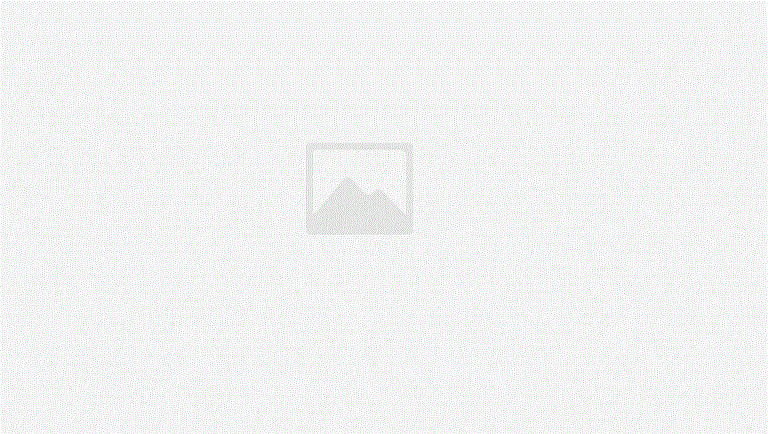
हमारा इतिहास
किसी भी संस्था के इतिहास का उद्देश्य उस संस्था की कार्यप्रणाली, घटनाओं, नीतियों और उसके संस्थागत विकास-क्रम का दस्तावेजीकरण, संदर्भों को जोड़ना, संकलन करना तथा एक व्यापक, प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रस्तुत करना है। केंद्रीय बैंक का संस्थागत इतिहास, कुछ मायनों में, देश के मौद्रिक इतिहास को दर्शाता है, जो नीतियों, विचारों, गलतियों, विचार-प्रक्रियाओं, निर्णय-प्रक्रियाओं और सामयिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था की व्यापक स्थिति को ठोस और मानवीय शब्दों में सामने लाता है।
इस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास न केवल भारत में केंद्रीय बैंकिंग के विकास-क्रम के बारे में बताता है, बल्कि यह संदर्भ के रूप में भी कार्य करता है और भारत के मौद्रिक, केंद्रीय बैंकिंग और विकास इतिहास के साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमने अब तक अपने इतिहास के पांच खंड प्रकाशित किए हैं।
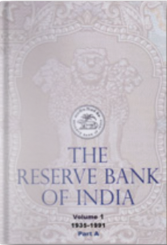
खंड 1
- (1935-1951)
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। यह अपने संस्थागत इतिहास का दस्तावेजीकरण करने वाले कुछ केंद्रीय बैंकों में से एक है। अब तक इसने अपने इतिहास के पांच खंड प्रकाशित किए हैं। खंड 1 1935 से 1951 तक की अवधि से संबंधित है, जिसे 1970 में प्रकाशित किया गया था। इसमें भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है और रिज़र्व बैंक के स्थापन के प्रारंभिक वर्षों को शामिल किया गया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता के बाद के युग के दौरान रिज़र्व बैंक और सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। यह अपने संस्थागत इतिहास का दस्तावेजीकरण करने वाले कुछ केंद्रीय बैंकों में से एक है। अब तक इसने अपने इतिहास के पांच खंड प्रकाशित किए हैं। खंड 1 1935 से 1951 तक की अवधि से संबंधित है, जिसे 1970 में प्रकाशित किया गया था। इसमें भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है और रिज़र्व बैंक के स्थापन के प्रारंभिक वर्षों को शामिल किया गया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता के बाद के युग के दौरान रिज़र्व बैंक और सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
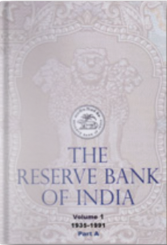
खंड 2
- (1951-1967)
1951 से 1967 तक की अवधि को शामिल करते हुए खंड 2 को 1998 में प्रकाशित किया गया। इस अवधि में भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास के युग की शुरुआत हुई। इस खंड में देश की आर्थिक और वित्तीय संरचना को मजबूत करने, संशोधित करने और विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख है। मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में रिज़र्व बैंक की भूमिका के अलावा, यह भारत में कृषि और दीर्घकालिक औद्योगिक ऋण के लिए एक संस्थागत अवसंरचना स्थापित करने के प्रयास पर प्रकाश डालता है। यह खंड देश के सामने आई बाहरी भुगतान समस्याओं और 1966 में हुए रुपये के अवमूल्यन को संक्षेप में बताता है।
1951 से 1967 तक की अवधि को शामिल करते हुए खंड 2 को 1998 में प्रकाशित किया गया। इस अवधि में भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास के युग की शुरुआत हुई। इस खंड में देश की आर्थिक और वित्तीय संरचना को मजबूत करने, संशोधित करने और विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख है। मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में रिज़र्व बैंक की भूमिका के अलावा, यह भारत में कृषि और दीर्घकालिक औद्योगिक ऋण के लिए एक संस्थागत अवसंरचना स्थापित करने के प्रयास पर प्रकाश डालता है। यह खंड देश के सामने आई बाहरी भुगतान समस्याओं और 1966 में हुए रुपये के अवमूल्यन को संक्षेप में बताता है।
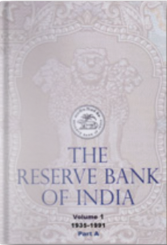
खंड 3
- (1967-1981)
18 मार्च 2006 को माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने रिज़र्व बैंक के इतिहास का तीसरा खंड जारी किया, जिसमें 1967 से 1981 तक की अवधि को शामिल किया गया है। इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना थी - 1969 में चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसके कारण देश के सुदूर क्षेत्रों में बैंकिंग का प्रसार हुआ। बैंकिंग में सुरक्षा और विवेकशीलता संबंधी मुद्दों को भी प्रमुखता मिली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली को त्यागने से भारत सहित विकासशील देशों के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हुईं। इस खंड में रिज़र्व बैंक और सरकार के बीच समन्वय के मामलों का भी उल्लेख है।
18 मार्च 2006 को माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने रिज़र्व बैंक के इतिहास का तीसरा खंड जारी किया, जिसमें 1967 से 1981 तक की अवधि को शामिल किया गया है। इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना थी - 1969 में चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसके कारण देश के सुदूर क्षेत्रों में बैंकिंग का प्रसार हुआ। बैंकिंग में सुरक्षा और विवेकशीलता संबंधी मुद्दों को भी प्रमुखता मिली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली को त्यागने से भारत सहित विकासशील देशों के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हुईं। इस खंड में रिज़र्व बैंक और सरकार के बीच समन्वय के मामलों का भी उल्लेख है।
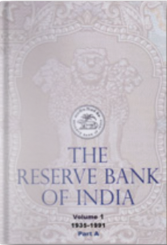
खंड 4
- (1981-1997)
रिज़र्व बैंक के इतिहास के खंड 4 का विमोचन भी भारत के माननीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 17 अगस्त 2013 को किया गया। यह 1981 से 1997 तक की 16 वर्षों में हुई विभिन्न घटनाओं से संबंधित है और इसे दो भागों में प्रकाशित किया गया है: भाग क और भाग ख, जिसे आदर्श रूप से निरंतरता में पढ़ा जाना चाहिए। भाग क प्रतिबंधों जैसी व्यवस्था से प्रगतिशील उदारीकरण तक भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन पर केंद्रित है। 1980 के दशक की विशेषता एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति थी जिसमें बजटीय घाटे का स्वचालित मुद्रीकरण हुआ, जिससे मौद्रिक नीति के संचालन पर तनाव पड़ा। इसी तरह, अति विनियमित बैंकिंग प्रणाली के कारण दक्षता पर प्रतिकूल असर पड़ा। बिगड़ती बाहरी स्थितियों और घरेलू समष्टि आर्थिक असंतुलन ने 1991 के भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट को जन्म दिया। बाद के सुधारों से न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि केंद्रीय बैंकिंग में भी दूरगामी परिवर्तन हुए। इस खंड के भाग ख में संरचनात्मक और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के कार्यान्वयन: राजकोषीय सुधार और स्वचालित मुद्रीकरण को समाप्त करना; सरकारी प्रतिभूति बाजार का विकास; और मुद्रा, प्रतिभूतियां और विदेशी मुद्रा बाजारों के बीच बेहतर एकीकरण का उल्लेख है। इसमें उदारीकरण और ऋण वितरण में सुधार के साथ बैंकिंग कार्य में हुए परिवर्तन को भी शामिल किया गया है। इसी दौरान, रिज़र्व बैंक को प्रतिभूति घोटाले से जूझना पड़ा, जिसके कारण बेहतर नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत हुई और भुगतान और निपटान प्रणालियों को मजबूत किया गया।
रिज़र्व बैंक के इतिहास के खंड 4 का विमोचन भी भारत के माननीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 17 अगस्त 2013 को किया गया। यह 1981 से 1997 तक की 16 वर्षों में हुई विभिन्न घटनाओं से संबंधित है और इसे दो भागों में प्रकाशित किया गया है: भाग क और भाग ख, जिसे आदर्श रूप से निरंतरता में पढ़ा जाना चाहिए। भाग क प्रतिबंधों जैसी व्यवस्था से प्रगतिशील उदारीकरण तक भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन पर केंद्रित है। 1980 के दशक की विशेषता एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति थी जिसमें बजटीय घाटे का स्वचालित मुद्रीकरण हुआ, जिससे मौद्रिक नीति के संचालन पर तनाव पड़ा। इसी तरह, अति विनियमित बैंकिंग प्रणाली के कारण दक्षता पर प्रतिकूल असर पड़ा। बिगड़ती बाहरी स्थितियों और घरेलू समष्टि आर्थिक असंतुलन ने 1991 के भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट को जन्म दिया। बाद के सुधारों से न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि केंद्रीय बैंकिंग में भी दूरगामी परिवर्तन हुए। इस खंड के भाग ख में संरचनात्मक और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के कार्यान्वयन: राजकोषीय सुधार और स्वचालित मुद्रीकरण को समाप्त करना; सरकारी प्रतिभूति बाजार का विकास; और मुद्रा, प्रतिभूतियां और विदेशी मुद्रा बाजारों के बीच बेहतर एकीकरण का उल्लेख है। इसमें उदारीकरण और ऋण वितरण में सुधार के साथ बैंकिंग कार्य में हुए परिवर्तन को भी शामिल किया गया है। इसी दौरान, रिज़र्व बैंक को प्रतिभूति घोटाले से जूझना पड़ा, जिसके कारण बेहतर नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत हुई और भुगतान और निपटान प्रणालियों को मजबूत किया गया।
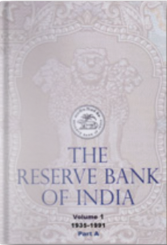
खंड 5
- (1997-2008)
भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास का पाँचवाँ खंड दिसंबर 2022 में जारी किया गया। इस खंड में 1997 से 2008 तक की 11 वर्ष की अवधि को शामिल किया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित इस खंड में आधिकारिक अभिलेखों, प्रकाशनों और इस अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक के कार्य से निकटता से जुड़े व्यक्तियों के साथ मौखिक चर्चा के आधार पर रिज़र्व बैंक का संस्थागत इतिहास शामिल है। यह खंड उक्त अवधि, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख संकटों, यानी एशियाई वित्तीय संकट और वैश्विक वित्तीय संकट द्वारा चिह्नित है, के दौरान प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में नीतियों और परिचालन में हुए परिवर्तनों के बारे में बताता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास का पाँचवाँ खंड दिसंबर 2022 में जारी किया गया। इस खंड में 1997 से 2008 तक की 11 वर्ष की अवधि को शामिल किया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित इस खंड में आधिकारिक अभिलेखों, प्रकाशनों और इस अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक के कार्य से निकटता से जुड़े व्यक्तियों के साथ मौखिक चर्चा के आधार पर रिज़र्व बैंक का संस्थागत इतिहास शामिल है। यह खंड उक्त अवधि, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख संकटों, यानी एशियाई वित्तीय संकट और वैश्विक वित्तीय संकट द्वारा चिह्नित है, के दौरान प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में नीतियों और परिचालन में हुए परिवर्तनों के बारे में बताता है।